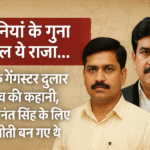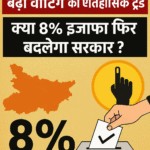जानिए भारत के 5 शहर जहाँ उठाए गए प्रदूषण नियंत्रण के सख्त कदम
समस्या
-
यहाँ कोयला खनन, कोक-उद्योग, तथा आसपास के औद्योगिक यूनिट्स वायु में बड़े मात्रा में धूल और कण (PM10/PM2.5) छोड़ते हैं।
-
शहर को 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की “नॉन-अटेनमेंट सिटी” में शामिल किया गया था।
कार्रवाई
-
क्षेत्रीय प्रशासन ने नए कोक-उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है क्योंकि ये वायु-प्रदूषण का स्रोत हैं।
-
शहर में धूल नियंत्रण, खनन-पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन तथा औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी बढ़ाई गयी है।
क्या आगे चाहिए
-
कोयला/कोक-उद्योगों को धीरे-धीरे स्विच करना चाहिए — जैसे स्वच्छ ऊर्जा या ग्रीन फ्यूल की ओर।
-
स्थानीय आबादी, स्कूल- बच्चों में वायु-प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव पर जागरूकता बढ़नी चाहिए।
-
औद्योगिक ज़ोन को शहर के बाहरी भागों में स्थानांतरित करने पर विचार हो सकता है ताकि आबादी सीधे प्रदूषण स्रोत के बहुत पास न हो।
2. तूथुकुडी (तमिलनाडु)
तूथुकुडी दक्षिण भारत का-एक ऐसा औद्योगिक केंद्र है जहाँ वायु-प्रदूषण विशेष रूप से ‘नॉन-अटेनमेंट’ श्रेणी में रहा है।
समस्या
-
इस शहर में थर्मल पावर प्लाँट्स, रासायनिक/ताम्र उद्योग और भारी-वाहन ट्रैफिक के कारण PM10 स्तर बहुत अधिक थे।
-
एनएएक्यूस के मुताबिक़, PM10 की अनुमति सीमा से काफी ऊपर था।
कार्रवाई
-
स्थानीय निगम द्वारा सड़क-सफाई, हरित पट्टी (green belt) और धूल नियंत्रण उपायों को मंजूरी दी गई।
-
परिणामस्वरूप, PM10 स्तर में ह्रास देखा गया है: 2017-18 में ~137 µg/m³ से घटकर 2023-24 में ~63 µg/m³।
क्या आगे चाहिए
-
कोयला-आधारित थर्मल पावर प्लाँट्स को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित करना।
-
ट्रैफिक नियंत्रण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।
-
परियोजनाओं की समय-समय पर मूल्यांकन एवं वायु-गुणवत्ता-डेटा की पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
3. आगरा (उत्तर प्रदेश)
आगरा भारत के उत्तर-यमुना क्षेत्र में एक प्रमुख शहर है, जहाँ वायु-प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर रही है।
समस्या
-
निर्माण-धूल, भारी ट्रैफिक, स्मॉग और आसपास कृषि अवशेष-जलने (stubble burning) जैसी समस्याओं के कारण यहां का वायु-गुणवत्ता बार-बार बहुत खराब होती रही है।
-
हाल के सर्वेक्षणों में आगरा को बड़े शहरों में तीसरा स्थान मिला हुआ है वायु-गुणवत्ता सुधार की दिशा में।
कार्रवाई
-
स्थानीय प्रशासन ने धूल-नियन्त्रण उपाय, पर्यावरण-निगरानी एवं औद्योगिक उत्सर्जन-नियमन बढ़ाया है।
-
निर्माण-स्थलों व ट्रैफिक-प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
क्या आगे चाहिए
-
कोयला-उपयोग वाली इकाइयों को अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत लाना (उदाहरण-स्वरूप थर्मल पावर प्लाँट्स, जनरेटर सेट्स)।
-
शहर के चारों ओर ट्रैफिक-वैकल्पिक मार्ग व पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाना।
-
नागरिकों में प्रदूषण-घटना (smog episode) के दौरान बचाव व्-उपायों की जानकारी का प्रसार।
4. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
कानपुर भी उत्तर भारत के बड़े औद्योगिक व आबादी-घनी शहरों में शामिल है, जहाँ वायु-प्रदूषण ने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।
समस्या
-
औद्योगिक उत्सर्जन, कोयला-उपयोग, मिश्रित ट्रैफिक तथा निर्माण-धूल यहां के प्रमुख कारक हैं।
-
हाल ही में रिपोर्टो में कानपुर को बड़े शहरों में पाँचवे स्थान पर रखा गया है वायु-गुणवत्ता सुधार की दिशा में।
कार्रवाई
-
स्थान-विशिष्ट वायु-प्रदूषण नियंत्रण योजनाएँ लागू की जा रही हैं।
-
ट्रैफिक प्रबंधन, निर्माण-धूल नियंत्रण तथा हरित पट्टी का विकास किया जा रहा है।
क्या आगे करना चाहिए
-
कोयला-जनित थर्मल पावर संयंत्रों व उद्योगों में शोध व निवेश बढ़ाना, साफ-उर्जा समाधान अपनाना।
-
जन-साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह बताना कि व्यक्तिगत स्तर पर कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं (जैसे निजी वाहन कम करना, मास्क का उपयोग, वायु-शुद्धिकरण…)।
-
शहर-आधारित वायु-गुणवत्ता-बैठकें व निगरानी समितियाँ गठित करना ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
5. मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
मुरादाबाद उत्तर भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में है, जिसे वायु-प्रदूषण के दृष्टिकोण से “नॉन-अटेनमेंट सिटी” माना गया है।
समस्या
-
शहर में उद्योग, ट्रैफिक और निर्माण-धूल के कारण PM10 का स्तर काफी ऊँचा रहा है।
-
उदाहरण के तौर पर, इसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उल्लेखनीय कार्य किया, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ बचे हुए हैं।
कार्रवाई
-
शहर ने 2017-18 के बाद से PM10 में 40 % से अधिक की कमी की श्रेणी में शामिल हुआ है।
-
स्थानीय प्रशासन ने निर्माण-धूल नियंत्रण, सड़क-सफाई व ट्रैफिक-उपायों को प्राथमिकता दी है।
भविष्य के सुझाव
-
कोयला-आधारित ऊर्जा व हीटिंग स्रोतों को स्वच्छ विकल्पों से बदलना।
-
औद्योगिक उत्सर्जन-निगरानी व्-सूचना प्रणाली को डिजिटल व अधिक पारदर्शी बनाना।
-
वायु-गुणवत्ता सुधार हेतु नागरिक भागीदारी (जैसे वायु-पोर्टल ऐप्स, शिकायत प्रकोष्ठ) को सक्रिय करना।
निष्कर्ष
यहाँ उल्लेखित पांच शहर — धनबाद, तूथुकुडी, आगरा, कानपुर व मुरादाबाद — यह दिखाते हैं कि वायु-प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। लेकिन ये उदाहरण यह भी हैं कि कार्रवाई संभव है और सुधार की दिशा में बदलाव आ सकते हैं। विशेष रूप से कोयला-उपयोग में कमी, स्वच्छ ईंधन अपनाना, निर्माण-धूल व ट्रैफिक-प्रबंधन जैसे उपाय अहम हैं।
अगर हम यह देखें कि दिल्ली-एनसीआर में कोयले के उपयोग पर बैन लगा है, तो अन्य शहरों को यह कदम प्रेरणा दे सकते हैं।
👉 आगे पढ़ें : बिहार चुनाव 2025 का सबसे चर्चित मर्डर केस: दुलारचंद यादव की हत्या और मोकामा का तनाव